*भूकंपों का वर्गीकरण*
भूकंप की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक भूकंप की अपनी अलग विशेषता होती है। भूकंपों की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण किया जाता है। इस लेख में हम विभिन्न आधार पर भूकंपों के वर्गीकरण का विवरण दे रहे हैं।
भूकंपों का वर्गीकरण
1. उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण (Classification earthquakes on the bases of depth of their focus)
भूकंपों के उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए ओल्डहम, गुटेनबर्ग, रिक्टर, बुल्लार्ड, बर्च आदि भू-वैज्ञानिकों ने कई अध्ययन किए हैं। ओल्डहम ने इटली के 5605 भूकंपों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 90% भूकंपों का उद्गम केन्द्र मूल भूपटल से 8 किमी। से कम गहराई पर होता है। 8% भूकंपों का उद्गम केन्द्र 8 से 30 किमी। की गहराई पर और केवल 2% भूकंपों का उद्गम केन्द्र 30 किमी। से अधिक गहराई पर स्थित होता है। अब तक 720 किमी। की अधिकतम गहराई पर उत्पन्न भूकंप के बारे में पता चला है। उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर भूकंपों को तीन वर्गों में बांटा जाता है:
(i) उथले भूकंप (Shallow Earthquakes): जिन भूकंपों का उद्गम केन्द्र 0 से 70 किमी। की गहराई पर होता है उन्हें उथले भूकंप कहते हैं। इन्हें साधारण भूकंप भी कहा जाता है। इन भूकंपों से जान-माल का अधिक नुकसान होता है। अधिकांश भूकंप इसी वर्ग के हैं।
(ii) मध्यवर्ती भूकंप (Intermediate Earthquakes): इन भूकंपों का उद्गम केन्द्र 70 से 300 किमी। की गहराई पर होता है।
(iii) गहरे भूकंप (Deep Earthquakes): ये भूकंप 300 से 720 किमी। की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें पातालीय (Plutonic) भूकंप कहते हैं और इनकी संख्या काफी कम होती है। अधिकांश गहरे भूकंप 500 से 700 किमी। की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।
2. उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण (Classification of earthquakes based on Origining Factors)
Why International Date Line Is Not A Straight Line? In Hindi
Why International Date Line Is Not A Straight Line? In Hindi
International Date Line marks the place where each day officially begins. At the international date line, the west side of the line has been always one day ahead of the East side, no matter what time of day it is when the line crossed.
(i) प्राकृतिक भूकंप (Natural Earthquakes): प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले भूकंपों को प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इनकी उत्पत्ति भूपटल को प्रभावित करने वाले अन्तर्जात बलों से होती है। प्राकृतिक भूकंप को चार उप-वर्गों में बांटा जाता है:
(a) संतुलन-मूलक भूकंप (Isostatic Earthquakes): जब कभी भूपृष्ठ के संतुलन में अव्यवस्था होती है तो भूगर्भिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और बलन पर्वतों के निर्माण के साथ-साथ भूकंप भी आते हैं। हिन्दु कोह में 1949 में आया भूकंप इसी प्रकार का था।
(b) ज्वालामुखी भूकंप (Volcanic Earthquakes): ज्वालामुखी उदगार के समय भूपृष्ठ में कंपन पैदा होता है और भूकंप आता है। विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में ही आते हैं। क्राकाटोआ (1833), कटमई (1912), एटना (1968) आदि ज्वालामुखी भूकंपों के उदाहरण हैं।
(c) वितलीय भूकंप (Plutonic Earthquakes): ऐसे भूकंपों का केन्द्र काफी गहराई (300 से 720 किमी।) में होता है। ऐसे भूकंप आंतरिक ऊष्मा द्वारा खनिजों के पुनर्गठन की क्रिया से उत्पन्न होते हैं।
(d) विवर्तनिक भूकंप (Tectonic Earthquakes): प्लेट विवर्तनिकी से नए भ्रंश बनते हैं और पुराने भ्रंशों पर गति करते हैं। इन घटनाओं से विवर्तनिक भूकंपों की उत्पत्ति होती है। सान फ्रांसिस्को (1906), जापान (1923) तथा कैलिफोर्निया की इम्पीरियल घाटी (1940) के भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक क्रिया से ही हुई थी।
(ii) कृत्रिम भूकंप (Artificial Earthquakes): ऐसे भूकंप मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य द्वारा भूतल के ऊपर तथा भूतल के नीचे किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी भूकंप आते हैं। खनिजों के लिए विस्फोट करने से तथा तेज गति से रेलगाड़ी के चलने से भी भूमि में कंपन पैदा होती हैं जिससे भूकंप आते हैं।
भूकंप की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक भूकंप की अपनी अलग विशेषता होती है। भूकंपों की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण किया जाता है। इस लेख में हम विभिन्न आधार पर भूकंपों के वर्गीकरण का विवरण दे रहे हैं।
भूकंपों का वर्गीकरण
1. उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण (Classification earthquakes on the bases of depth of their focus)
भूकंपों के उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर उनका वर्गीकरण करने के लिए ओल्डहम, गुटेनबर्ग, रिक्टर, बुल्लार्ड, बर्च आदि भू-वैज्ञानिकों ने कई अध्ययन किए हैं। ओल्डहम ने इटली के 5605 भूकंपों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि 90% भूकंपों का उद्गम केन्द्र मूल भूपटल से 8 किमी। से कम गहराई पर होता है। 8% भूकंपों का उद्गम केन्द्र 8 से 30 किमी। की गहराई पर और केवल 2% भूकंपों का उद्गम केन्द्र 30 किमी। से अधिक गहराई पर स्थित होता है। अब तक 720 किमी। की अधिकतम गहराई पर उत्पन्न भूकंप के बारे में पता चला है। उद्गम केन्द्र की गहराई के आधार पर भूकंपों को तीन वर्गों में बांटा जाता है:
(i) उथले भूकंप (Shallow Earthquakes): जिन भूकंपों का उद्गम केन्द्र 0 से 70 किमी। की गहराई पर होता है उन्हें उथले भूकंप कहते हैं। इन्हें साधारण भूकंप भी कहा जाता है। इन भूकंपों से जान-माल का अधिक नुकसान होता है। अधिकांश भूकंप इसी वर्ग के हैं।
(ii) मध्यवर्ती भूकंप (Intermediate Earthquakes): इन भूकंपों का उद्गम केन्द्र 70 से 300 किमी। की गहराई पर होता है।
(iii) गहरे भूकंप (Deep Earthquakes): ये भूकंप 300 से 720 किमी। की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें पातालीय (Plutonic) भूकंप कहते हैं और इनकी संख्या काफी कम होती है। अधिकांश गहरे भूकंप 500 से 700 किमी। की गहराई पर उत्पन्न होते हैं।
2. उत्पत्ति के कारकों के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण (Classification of earthquakes based on Origining Factors)
Why International Date Line Is Not A Straight Line? In Hindi
Why International Date Line Is Not A Straight Line? In Hindi
International Date Line marks the place where each day officially begins. At the international date line, the west side of the line has been always one day ahead of the East side, no matter what time of day it is when the line crossed.
(i) प्राकृतिक भूकंप (Natural Earthquakes): प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले भूकंपों को प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इनकी उत्पत्ति भूपटल को प्रभावित करने वाले अन्तर्जात बलों से होती है। प्राकृतिक भूकंप को चार उप-वर्गों में बांटा जाता है:
(a) संतुलन-मूलक भूकंप (Isostatic Earthquakes): जब कभी भूपृष्ठ के संतुलन में अव्यवस्था होती है तो भूगर्भिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और बलन पर्वतों के निर्माण के साथ-साथ भूकंप भी आते हैं। हिन्दु कोह में 1949 में आया भूकंप इसी प्रकार का था।
(b) ज्वालामुखी भूकंप (Volcanic Earthquakes): ज्वालामुखी उदगार के समय भूपृष्ठ में कंपन पैदा होता है और भूकंप आता है। विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्रों में ही आते हैं। क्राकाटोआ (1833), कटमई (1912), एटना (1968) आदि ज्वालामुखी भूकंपों के उदाहरण हैं।
(c) वितलीय भूकंप (Plutonic Earthquakes): ऐसे भूकंपों का केन्द्र काफी गहराई (300 से 720 किमी।) में होता है। ऐसे भूकंप आंतरिक ऊष्मा द्वारा खनिजों के पुनर्गठन की क्रिया से उत्पन्न होते हैं।
(d) विवर्तनिक भूकंप (Tectonic Earthquakes): प्लेट विवर्तनिकी से नए भ्रंश बनते हैं और पुराने भ्रंशों पर गति करते हैं। इन घटनाओं से विवर्तनिक भूकंपों की उत्पत्ति होती है। सान फ्रांसिस्को (1906), जापान (1923) तथा कैलिफोर्निया की इम्पीरियल घाटी (1940) के भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक क्रिया से ही हुई थी।
(ii) कृत्रिम भूकंप (Artificial Earthquakes): ऐसे भूकंप मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य द्वारा भूतल के ऊपर तथा भूतल के नीचे किए जाने वाले विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी भूकंप आते हैं। खनिजों के लिए विस्फोट करने से तथा तेज गति से रेलगाड़ी के चलने से भी भूमि में कंपन पैदा होती हैं जिससे भूकंप आते हैं।











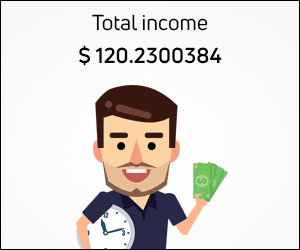

0 Comments